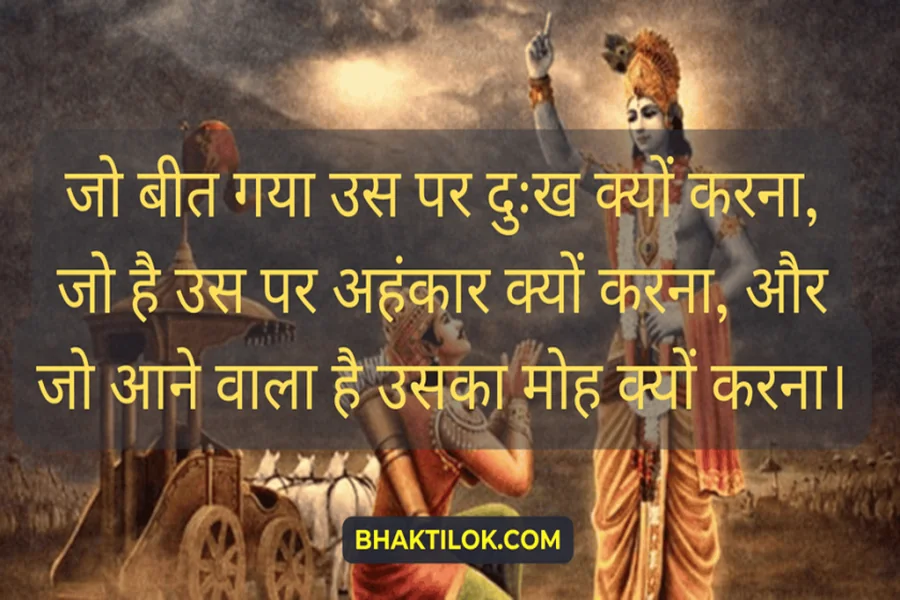
भगवद गीता के कर्म उद्धरण हिंदी में
-
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥”
— (अध्याय 2, श्लोक 47)
अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा न करो, और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। -
“योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥”
— (अध्याय 2, श्लोक 48)
अर्थ: हे धनंजय! योग की स्थिति में रहकर, समभाव से सफल और असफल में समान दृष्टि रखकर कर्म करो। यही योग है। -
“नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 5)
अर्थ: कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता क्योंकि सभी को प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करना पड़ता है। -
“कर्म करो लेकिन फल की इच्छा त्याग दो। यही सच्चा कर्मयोग है।”
— सारांश -
“इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्यार्थेभ्यः समाहितः।
असक्तः सर्वकर्माणि विद्ध्यात्मैवात्मनात्मनः॥”
— (अध्याय 5, श्लोक 8)
अर्थ: जो मनुष्य इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से लगाव से मुक्त रखता है और अपने आप में स्थित रहता है, वही सब कर्मों में असक्त होता है। -
“कर्म करो, परन्तु फल की इच्छा मत करो। फल की आशा मन को भ्रमित करती है।”
— (अध्याय 2, श्लोक 49 का भावार्थ) -
“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 35)
अर्थ: अपने स्वधर्म का पालन करना, भले वह दोषपूर्ण हो, परधर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना बेहतर है, क्योंकि परधर्म भयावह है। -
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥”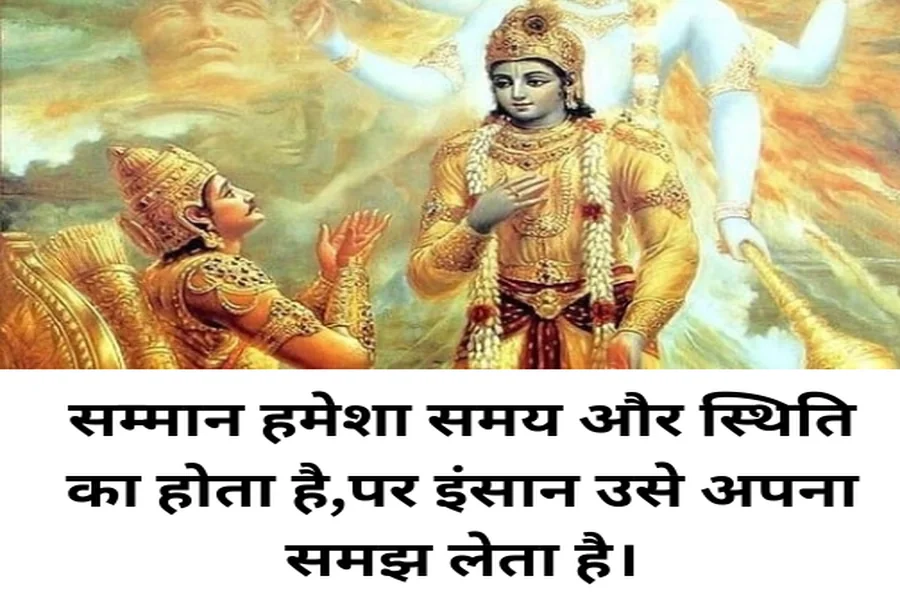
— (अध्याय 18, श्लोक 66)
अर्थ: सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए चिंता मत करो। -
“कर्म करता रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता छोड़ दो और समभाव से कार्य करो।”
— (गीता का सारांश) -
“योगी युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा सर्वत्र समः।
अचलं कर्मणि मनःः संयमात्मा जितेन्द्रियः॥”
— (अध्याय 5, श्लोक 12)
अर्थ: जो योगी फल की इच्छा त्याग कर सभी स्थानों पर समान मन से कर्म करता है, जिसका मन अचल और संयमित होता है, वह इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है। -
“हे अर्जुन! कर्म ही जीवन का आधार है। इसे छोड़कर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है।”
— (अध्याय 3 का सारांश) -
“जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सर्वदा शांति में रहता है।”
— (गीता की शिक्षा) -
“धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।”
— (अध्याय 4, श्लोक 7)
अर्थ: धर्म की स्थापना के लिए मैं युग-युग में पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। -
“कर्म का दण्ड उसके फल में नहीं, कर्म के त्याग में है। जो कर्म त्याग करता है, वह कायर कहलाता है।”
— (अध्याय 3, श्लोक 9 का भावार्थ) -
“तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 19)
अर्थ: इसलिए हे पुरुष, बिना किसी आसक्ति के हमेशा अपने कर्म करते रहो। आसक्ति रहित कर्म करने वाला परम पुरुष श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। -
“यज्ञार्थात्कर्मणो’nyत्र लोकस्य न कर्मणः कुतः।
कर्मण्यभिप्रेत्य तत्त्वं त्यक्त्वा न स विशिष्यति॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 9)
अर्थ: संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, बिना कर्म के कोई भी जीव नहीं रह सकता। इसलिए कर्मों को त्यागना संभव नहीं, परन्तु कर्मों को यज्ञ के लिए समर्पित करना श्रेष्ठ है। -
“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥”
— (अध्याय 2, श्लोक 38)
अर्थ: सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान मानकर, तू युद्ध में लग जा, ऐसा करके तू पाप से बच जाएगा। -
“नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 8)
अर्थ: तुम्हें अपना निर्धारित कर्म करना चाहिए, निष्क्रिय रहने से कर्म अधिक है। शरीर के चलने-फिरने के लिए भी कर्म करना जरूरी है, निष्क्रियता से सफलता नहीं मिलती। -
“एवं सततयुक्ता योगिनो विनियतात्मनः।
श्रद्धावान्भजतात्मानं स मे युक्ततमा मतिः॥”
— (अध्याय 6, श्लोक 47)
अर्थ: जो योगी निरंतर संयमित और आत्म-नियंत्रित रहता है और विश्वासपूर्वक मुझे भजता है, वह मेरी सबसे योग्य इच्छा वाला है। -
“कर्मों से कभी डरो मत, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। पर कर्म करो निष्काम भाव से।”
— (गीता का सारांश) -
“कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो मनुष्य कर्म में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी होता है।”
— (अध्याय 2, श्लोक 47 का सारांश) -
“मोहात्ते मां मतपराधीं तत्कर्म प्रविधीयते।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 30)
अर्थ: जो मुझ पर विश्वासघात करता है और मुझसे दूर रहता है, उसके कर्म व्यर्थ होते हैं। इसलिए, सब कर्मों को त्यागकर मुझमें समर्पित हो जाओ। -
“कर्मफल-त्यागी सदा हरि भजन करता है और संसार के बंधनों से मुक्त होता है।”
— (गीता की शिक्षा) -
“तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 19)
अर्थ: बिना आसक्ति के हमेशा कर्म करते रहो। जो ऐसा करता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। -
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥”
— (अध्याय 3, श्लोक 21)
अर्थ: जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वही दूसरे लोग भी करते हैं। लोग उसी के अनुसार कर्म करते हैं। -
“कर्म कर्मेति कहि संरभो न संन्यासे कुटुम्बकम्।
अविवेक्य पुरुषार्थं प्राप्य कर्माणि न त्यजेत्॥”
— (अध्याय 18, श्लोक 5)
अर्थ: कर्म को त्यागना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कर्मों को छोड़ नहीं देता। -
“हे अर्जुन! मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे मन में संशय है, परंतु तुम्हें अपने कर्मों का पालन करना है।”
— (अध्याय 2 का सारांश) -
“कर्मों का पालन करना जीवन का परम उद्देश्य है, और फल को त्यागना कर्मयोग का सार है।”
— (गीता का सारांश) Best Nanad Bhabhi Quotes 2025 -
“तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का प्रतिबिम्ब है, इसलिए सही कर्मों का चुनाव करो।”
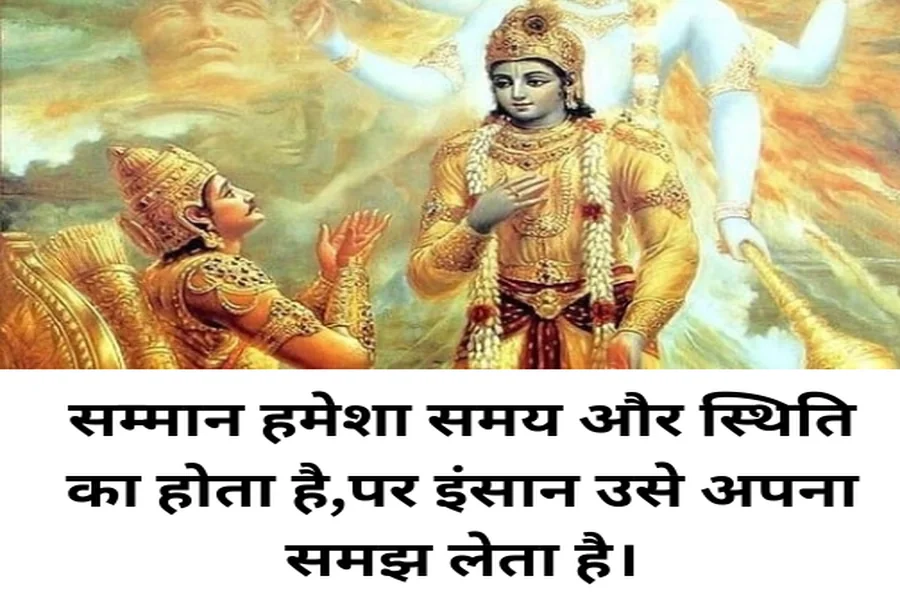
— (गीता की शिक्षा) -
“सततं कर्म समाचर, सफलता स्वयंसिद्ध होगी।”
— (गीता का उपदेश) -
“जो लोग अपने कर्मों के फल को त्याग कर बिना किसी उम्मीद के कर्म करते हैं, वे ही सच्चे कर्मयोगी होते हैं।”
— (अध्याय 3, श्लोक 19 का सारांश) -
“कर्म करने का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, न कि केवल भौतिक फल की प्राप्ति।”
— (भगवद गीता की शिक्षा) -
“साधक का कर्म हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है।”
— (गीता का संदेश) -
“निराशा और आलस्य का त्याग कर, कर्मों में पूरी शक्ति और उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए।”
— (गीता का उपदेश) -
“कर्म करते समय अपने मन और इन्द्रियों को नियंत्रित करना, यही सच्चा योग है।”
— (अध्याय 3, श्लोक 7) -
“कर्म और ज्ञान दोनों को साथ-साथ लेकर चलने से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है।”
— (गीता का संदेश) -
“जो अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह शांति और संतोष प्राप्त करता है।”
— (अध्याय 9, श्लोक 22) -
“यदि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तो उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्मयोग है।”
— (अध्याय 2, श्लोक 47 का सारांश) -
“कर्म न करने से नहीं, बल्कि कर्म में भागीदारी से सच्ची सफलता मिलती है।”
— (गीता का उपदेश) -
“सच्चे कर्मी वे होते हैं जो अपने कार्यों को निष्कलंक और निष्कलुष रूप से करते हैं, बिना किसी लोभ और स्वार्थ के।”
— (भगवद गीता के श्लोक) -
“कर्म से मत डर, क्योंकि कर्म करना जीवन का उद्देश्य है। निष्कलंक कर्म करने से ही आत्मा शुद्ध होती है।”
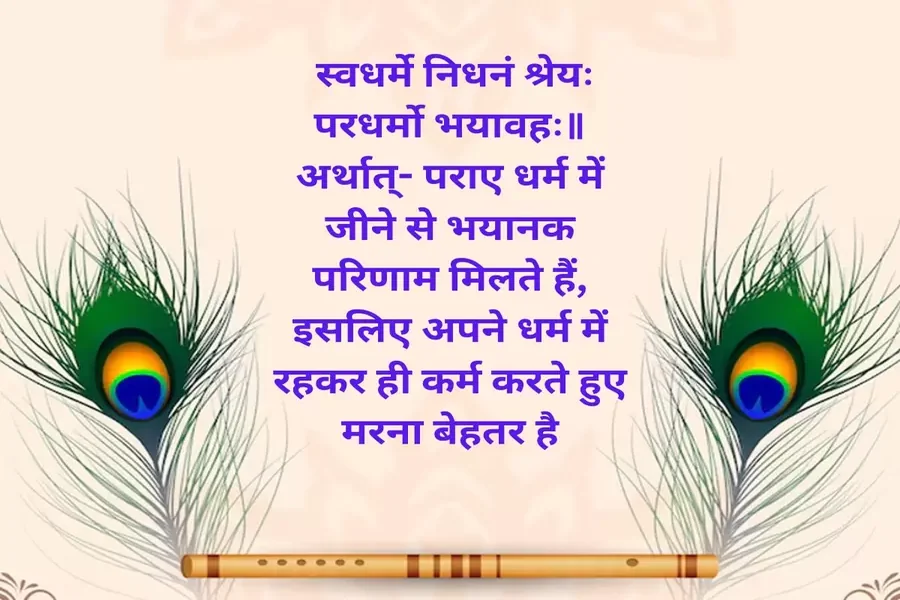
— (अध्याय 3, श्लोक 35 का सारांश) -
“निरंतर कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है, क्योंकि फल तो परमात्मा के हाथ में है।”
— (अध्याय 2, श्लोक 47) -
“जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है।”
— (अध्याय 9, श्लोक 22) -
“मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी भी अपने मन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं, आत्मिक उन्नति है।”
— (गीता की शिक्षा) -
“स्वधर्म में कर्म करने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे का धर्म निभाने से नुकसान ही होगा।”
— (अध्याय 3, श्लोक 35) -
“कर्म करते समय यदि मन और इन्द्रियों पर नियंत्रण हो, तो मनुष्य अपने कर्म में सफल होता है।”
— (अध्याय 6, श्लोक 47) -
“कर्म करने में मन की ईमानदारी और समर्पण बहुत जरूरी है, तभी कर्म सही मार्ग पर होगा।”
— (गीता की शिक्षा) -
“कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि एक साधना है, जो आत्मा को शुद्ध और उन्नत बनाती है।”
— (अध्याय 3, श्लोक 16) -
“जो कर्मयोगी होता है, वह जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य से करता है और हर स्थिति में स्थिर रहता है।”
— (अध्याय 5, श्लोक 7) -
“कर्म न केवल परिवार के लिए किया जाता है, बल्कि समाज और आत्मा के लिए भी किया जाता है।”
— (गीता का सारांश)